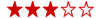'आर्टिकल 15 सिर्फ नकल या अख़बारों की हेडलाइन्स से उठाया गया प्लॉट नहीं है।'
'यह पूरे रीसर्च के साथ बनाई गयी एक अच्छी फिल्म है; और इसमें दिखाई गयी बातों के पीछे एक मक़सद है,' श्रीहरि नायर का कहना है।

मूवी जॉनर पहचानने के खेल में मैं कच्चा हूं; लेकिन इस बार मैं इस खेल को खेले बिना रह नहीं पाया।
आर्टिकल 15 में, डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने अपने सामाजिक प्रयासों के अलावा, पल-पल हमें उनके सिनेमैटिक अंदाज़ का भी एहसास दिलाया है। यह ईमानदार पुलिसवाले और अपराधी के टकराव की बेहतरीन कहानी है, जिसमें हास्य को बहुत ही ख़ूबसूरती से पिरोया गया है।
हमें पहले से पता होता है कि चुनौतियों से भरे लालगाँव में तैनात किये गये नये-नये आइपीएस ऑफ़िसर अयान रंजन (आयुष्मान खुराना) को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हम पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिस्टम की बेरहमी, जाति-आधारित राजनीति और उसके अपने विभाग के पाखंड से वो निराश हो जायेगा।
लेकिन अनुभव सिन्हा की कहानी में अद्भुत अंदाज़ में परोसे गये हास्य और विरोधाभास का हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, और यही बात पूरी फिल्म में हमें रोमांचित करती है।
हम पुलिसवालों की पुरानी फिल्में देखते आये हैं और स्वाभाविक है कि हम मुख्य किरदार की ईमानदारी और पवित्रता की तरफ़दारी करेंगे। लेकिन यहाँ, अयान रंजन की पवित्र सोच और फिर पवित्र जीवन में घुलने वाला रोमांस उसे एक मूर्ख के रूप में दिखाता है, जिसने अपनी काबिलियत से कहीं ज़्यादा बड़ा काम हाथ में ले लिया है।
रंजन के इलाके में दो लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और तीसरी लड़की लापता हो जाती है; लेकिन उनके ऑफ़िशियल हेडक्वॉर्टर में प्लम्बिंग की समस्याओं को दूर करना और बात-चीत में दखल देने वाले एक शोर मचाते पंखें को ठीक कराना गंभीर मुद्दे हैं।
आयुष्मान खुराना को अपनी इस छवि से बाहर आते देखना अच्छा लगता है: खुराना के रोल अक्सर विडंबना का एहसास देते हैं। 'किरदार में डूब जाना' उनकी ताक़त नहीं है (इस तरह का विश्लेषण उन आलोचकों की पहचान है, जो साधारण उक्तियों से आगे बढ़कर बात नहीं कर सकते)।
आयुष्मान खुराना के बेहतरीन परफॉर्मेंसेज़ में, आप उन्हें स्क्रिप्ट में दिये गये किरदार को मुस्कुराहट के साथ ख़ुद में उतारता हुआ महसूस कर सकते हैं; मानो वो उस किरदार के हर उतार-चढ़ाव को सूंघ लेते हों -- और यही बात दर्शकों का दिल जीत लेती है और हम उनके इस खेल के प्यादे बन जाते हैं।
यहाँ भी, अभिनेता ख़ाकी वर्दी और चौड़ी मूछों में खो नहीं जाता। और हमें पता होता है कि हमसे झूठ कहा जा रहा है और 'अभिनेता के डूब जाने' जैसी कोई बात न होने के कारण ही अयान रंजन का किरदार दर्शकों को भाता है। (साधारण आदर्शवादी पुलिसवाला 2019 में शायद चल नहीं पाता; लेकिन यह हल्की सी धोखेबाज़ी ज़रूर रंग लाई है)।
फिल्म के आगे बढ़ने पर, अयान रंजन को पता चलता है सिस्टम कितनी गहराई तक सड़ चुका है। लेकिन अनुभव सिन्हा ने इसी साधारण सी कहानी में ख़ूबसूरती को ज़िंदा रखा है: उन्होंने रंजन और उसके पुलिस स्टेशन के आस-पास इतनी गंदगी फैलाई है कि कहानी को दिशा देने से पहले इस गंदग़ी को साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है।
और सफ़ाई के काम का धीमापन और नौसीखिया अंदाज़, आने वाली कई अड़चनें भी रंजन और उसकी टीम की खोई हुई लड़की को ढूंढने की कोशिशों का हिस्सा हैं -- और यही बात आर्टिकल 15 की कहानी को एक अलग स्वाद देती है।
यूं तो मुख्य कहानी में दिखाने के लिये ज़्यादा कुछ नहीं है; लेकिन अनुभव सिन्हा ने इस फिल्म को परिहास और ख़ूबसूरती से भर दिया है।
एक बहुत ही मज़ेदार सीन में रंजन की पुलिस टीम आपस में बात करती है कि पिछले चुनावों में उन्होंने किसे वोट दिया था। और जल्द ही चर्चा उम्मीदवारों से उनके चुनाव चिह्नों तक पहुंच जाती है। 'मुझे तो पुल पसंद है। लेकिन पुल नहीं था, तो बल्ब को वोट देना पड़ा,' एक पुलिस वाला आवाज़ में बिना किसी व्यंग्य के कहता है।
सिन्हा आज की तारीख में देश के बेहतरीन डायलॉग राइटर्स में से एक हैं (मैं उन्हें श्याम पुष्करण और विशाल भारद्वाज के स्तर पर देखता हूं); और उनकी लाइन्स, उनका मज़ाकिया अंदाज़ मुख्य विषय को एक अलग चेहरे के साथ हमारे सामने पेश करता है - क्योंकि अगर हम सिस्टम की लाचारी का मज़ाक उड़ा सकते हैं, तो उसे सहन भी कर ही सकते हैं।
डायलॉग्स तो मज़ेदार हैं ही, लेकिन कहानी का व्यावहारिक हास्य भी हमें गुदगुदाता रहता है।
एक ऊंचे ओहदे वाला पुलिस अधिकारी एक कार्यक्रम से जाने के लिये तैयार हो जाता है, और दो सेकंड इंतज़ार करता है ताकि निचले पद वाले पुलिसकर्मी उसके पैर छू सकें।
अयान रंजन अपने सस्पेंशन ऑर्डर पर साइन करते हैं, और उसे दो जूनियर ऑफ़िसर्स को सौंप देते हैं, और फिर थोड़ी देर जूनियर्स ऑफ़िसर्स के सलाम ठोंकने के लिये रुकते हैं।
सिन्हा और उनके को-राइटर जानते हैं कि भावनात्मक गंभीरता के बीच नौकरशाही की परंपराओं को घड़ी के काँटों की तरह चलते देखना कितना मज़ेदार हो सकता है। लेखक ने पूरी कहानी में इस रस को छिड़का है।
फिर बारी आती है आईनों की।
एक सोशलिस्ट (मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब द्वारा निभाया गया किरदार) बताता है कि कैसे क्रांति के प्रति उनके समर्पण के कारण वो अपनी प्रेमिका (सयानी गुप्ता द्वारा निभाया गया किरदार) को प्यार के पल नहीं दे पाया। कुछ सीन्स के बाद अयान रंजन अपनी पत्नी (ईशा तलवार) से माफी मांगते नज़र आते हैं क्योंकि वो कभी एक क्रांतिकारी नहीं बन पाये, जैसा उनकी पत्नी चाहती थीं।
ऐसा लगता है कि आर्टिकल 15 की कहानी का जन्म इन्ही हसरतों से हुआ है: जैसे सिन्हा ने इस फिल्म की कहानी अपने बचपन की किसी जगह पर जाते-जाते सोची हो।
फिल्म के दृश्यों में भी 'पलट कर देखने का एहसास' साफ़ झलकता है -- आर्टिकल 15 की झलक एक सपने की तरह है; जैसे अतीत की कोई याद।
सिन्हा भी दृश्यों के बीच वक़्त के साथ खेलते दिखाई देते हैं।
बलात्कार का एक आरोपी 'औक़ात' की बात करता दिखाई देता है -- और बीच में ही एक फोन की घंटी हमारी धड़कनें तेज़ कर देती है। ख़ून के साथ-साथ एक राज़ को सामने लाने वाली हिंसा की एक घटना इतनी तेज़ी से होती है, कि मेरे हलक़ से चीख निकल गयी।
हिंसा के असर को प्रभाववादी ढंग से दिखाया गया है; और साथ-साथ चलती एडिटिंग में भी यही अंदाज़ उभर कर आता है। जब कोई पुलिस वाला अपनी जान ले लेता है, तो हम इसी चीज़ को दूसरे पुलिस वाले के भीतर चलता देखते हैं।
इस मूवी में मर्द ऐसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं और इनसे प्रभावित होते हैं; लेकिन महिलाओं के चेहरों पर एक संवेदनहीनता दिखाई देती है, जो लगातार हिंसा के बीच रहने से आई है।
सयानी गुप्ता एक बार फिर पीड़ितों के भावहीन प्रतीक के रूप में दिखाई देती हैं; और ईशा तलवार फरिश्तों की ख़ामोशी दर्शाती हैं: वो अयान रंजन की अंतरात्मा पर हावी अंतरात्मा हैं।
मुझे लगता है अनुभव सिन्हा अपने पसंदीदा अभिनेताओं की एक कंपनी बना रहे हैं; और अगर ऐसा है, तो मनोज पहवा और कुमुद मिश्रा उस कंपनी का अहम हिस्सा हैं।
मोटापे में एक जैसे, पहवा और मिश्रा यहाँ मैकबेथ की चुड़ैलों के जैसा किरदार निभा रहे हैं; जिनके बीच बस जाति का अंतर है (पहवा का किरदार ब्रह्मदत्त ऊंची जाति वाले तबके का इंस्पेक्टर है), और दूसरा अंतर यह है कि एक ने अपनी आवाज़ को पूरी तरह दूसरे के सामने दबा दिया है (मिश्रा का किरदार अपनी उम्र के 50 के दशक में है और अभी भी नीची जाति के दबे हुए वातावरण में जी रहा है)।
ये दोनों ही ख़ूबसूरत किरदार हैं।
ब्रह्मदत्त की चाल-ढाल और भाषा सिस्टम के भेदभाव के अनुसार बिल्कुल सही ढल गयी है; और ख़ुद को बड़ा दिखाने के लिये वह भूखे कुत्तों को बिस्किट खिलाता है। वह कोई खोखला खलनायक नहीं है और दलित राजनेता के बारे में बात करते हुए फिल्म की सबसे ख़ूबसूरत बात कहता है: 'जब पावर में होते हैं, तो मूर्तियाँ बनवाते हैं; जब विपक्ष में होते हैं, तो फिर से दलित बन जाते हैं।'
कुमुद मिश्रा के चेहरे पर बाबुओं वाली मुश्किलों से भरी मुस्कान दिखाई देती है; और उन्हें फिल्म का सबसे मज़ेदार सीन मिला है। लेकिन पूरी फिल्म में वो कुमुद मिश्रा वाली चीज़ें भी करते दिखाई देते हैं: जैसे पीछा करते हुए बीच में रुक जाना और खड़े होकर दूर कहीं देखना।
फिल्म ख़त्म होते-होते मिश्रा का किरदार पहवा के किरदार से अपना बदला ले लेता है, और उस थप्पड़ से मेरे बगल की सीट पर बैठी लड़की खुशी से चिल्ला उठी!!!
ख़ुशी से चिल्लाती लड़की ने शायद यह नहीं देखा कि मिश्रा बाद में अपनी ऊंची जाति के बॉस को थप्पड़ मारने के लिये रोते दिखाई देते हैं। जीत तो मिली, लेकिन उसके साथ आये पछतावे का क्या करें?
लेकिन, आर्टिकल 15 में आपको ख़ुशी के मारे निकली दर्शकों की चीखें कई बार सुनाई देंगी: क्योंकि मूवी भीड़ को ख़ुश करने के लिये ही बनाई गयी है। और जहाँ तक भीड़ को ख़ुश करने की बात है, यह फिल्म अपने शहरी, पढ़े-लिखे दर्शकों को पहचानती है और जानती है कि कौन सी बात उन्हें ख़ुश करती है।
मैं देखना चाहूंगा कि आदिवासी समुदाय, मान लीजिये छत्तीसगढ़ से, इस फिल्म पर क्या प्रतिक्रिया देता है। और फिल्म की यही चतुराई इसे एक महान फिल्म बनने से रोकती है।
क्योंकि इसकी सोच और मस्ती के बावजूद हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 15 की हर चीज़ हमारी बनावटी भावुकता को संतुष्ट करने के लिये बुनी गयी है।
हमें बस आराम से बैठकर मूवी की हर चीज़ को देखना है, और पर्दे पर दिखाये जा रहे हर उतार-चढ़ाव पर ख़ुशी से चीख कर अपने भीतर के अच्छे इंसान को तसल्ली देनी है। साथ ही मूवी का परेड म्यूज़िक, जिसे खतरे की घंटी का रूप दिया गया है, हमारे ज़ेहन को और भी झकझोरता है।
आर्टिकल 15 सिर्फ नकल या अख़बारों की हेडलाइन्स से उठाया गया प्लॉट नहीं है। यह पूरे रीसर्च के साथ बनाई गयी एक अच्छी फिल्म है; और इसमें दिखाई गयी बातों के पीछे एक मक़सद है।
अनुभव सिह्ना ने मज़बूती से अपने कदम जमाये हैं ताकि मल्टिप्लेक्स में भीड़ जुटाना आसान हो सके। (मुझे उम्मीद है कि मूवी काफ़ी पैसे कमायेगी; क्योंकि इसे 'सामाजिक बुराइयों' पर जीत पाने के साथ-साथ अपने निर्माताओं के प्रति आर्थिक ज़िम्मेदारियों का भी ध्यान रखते हुए बनाया गया है)।
पिछले कुछ सालों में भारत के अन्य उद्योगों की तरह बॉलीवुड मूवीज़ के स्तर भी काफी बदल गये हैं। और इनमें से एक बदलाव यह भी है कि जिस फिल्म को 15 साल पहले मसाला फिल्म कहा जाता था, आज उसे बी-मूवी कहा जाता है -- जबकि मसाला फिल्मों की जगह अब अलग तरह की फिल्मों ने ले ली है।
पूरे सिस्टम को अकेले हरा देने वाला हीरो भले ही अच्छी ओपनिंग हासिल कर ले; लेकिन मसाला सिनेमा की असली क्वॉलिटी अब सामाजिक उद्देश्यों पर बनी फिल्मों में ही दिखाई देती है।
तो पिंक, मुल्क़, और अब आर्टिकल 15 आज की मसाला फिल्में हैं (आर्टिकल 15 निश्चित रूप से तीनों में से सबसे अच्छी है)। और आज के ज़माने की इन फिल्मों का विजेता हीरो इनके भीतर छुपा सामाजिक उद्देश्य है।
यह बदलाव अभी उतना स्पष्ट नहीं हुआ है कि इसे एक ट्रेंड कहा जा सके; लेकिन इन फिल्मों की सिनेमैटिक तकनीक इस सच को हमारे सामने रखती है।
जैसे इस फिल्म के सबसे ज़बर्दस्त सीन में कोई हीरो सीना ताने कैमरे की ओर बढ़ता नहीं दिखाई देता, बल्कि खुराना के हाथ से संविधान के आर्टिकल 15 की एक कॉपी स्लो मोशन में उड़ती हुई दिखाई देती है।
यह काग़ज़ का टुकड़ा हो, पिंक के लैंगिक समानता पर दिये गये भाषण हों, या फिर मुल्क़ में दिखाया गया सांप्रदायिक भाईचारा हो, ये सभी ऐसे वीर नायक हैं, जिनकी ताक़त पर आप सवाल नहीं उठा सकते।
जी हाँ! एक सामाजिक उद्देश्य आज के दौर में पैसे बनाने की उतनी ही ताकतवर पूंजी है, जितनी 15 साल पहले सुपरस्टार की मौजूदग़ी हुआ करती थी।
सिन्हा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, और वो लगातार अपनी तकनीक को बेहतर बनाते जा रहे हैं, और अपनी टीम जुटा रहे हैं; लेकिन उनके काम में और भी ज़्यादा भावुकता होती, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता।
ग़लत-सही में फर्क समझने वाली जनता को ख़ुश करने वाला फिल्म-मेकर, जो ख़ास तौर पर हमारे भीतर के ग़ुस्से को आग देता है, क्या उसे हम कलाकार कह सकते हैं? मैं इसपर अपना फैसला नहीं सुनाना चाहूंगा।
आर्टिकल 15 के मुख्य किरदारों को ख़ूबसूरती से बनाया गया है -- सिन्हा ने ध्यान रखा है कि किसी भी किरदार के हिस्से में समझदारी कम न पड़े। लेकिन बैकग्राउंड में मौजूद किरदारों ने सहानुभूति और दया की भावना जगाने से ज़्यादा कोई काम नहीं किया है।
इसलिये, जब भेड़-बकरियों की तरह दिखाये गये इन लोगों के हालात पर भाषण दिये जाते हैं और अर्थपूर्ण चिह्नों के साथ उनपर अभियान निकाले जाते हैं, तो इन सब में थोड़ा सा पाखंड ज़रूर दिखाई देता है।
मूवी बरसात में शूट किये एक गाने से शुरू होती है -- जिसमें निचली जातियों के कुछ लोग उनके साथ हुए अन्याय को याद करते हैं।
वास्तव में ये सभी गाने लोकगीत बन जाते हैं, इनमें से बहुत से गाने बच्चों की लोरियों का भी रूप ले लेते हैं -- और जहाँ एक ओर हम शहरी लोग उनमें मौजूद दर्द को देख कर आहें भरते हैं, वहीं दूसरी लोग इस दर्द को झेल चुके लोगों के लिये ये गाने एक तरह की ताकत का स्रोत होते हैं।
अनुभव सिन्हा समझते हैं कि इस तरह के विरोधाभास हमारे समाज में साफ़ दिखाई देते हैं; लेकिन अभी वो भी एक गहरी सोच वाले व्यक्ति के रूप में अपनी छवि को मज़बूत करने में लगे हैं -- जो हमारे मेनस्ट्रीम सिनेमा में उनके 17 साल के फिल्म-मेकिंग करियर में अभी तक नहीं हो पाया था।
मुझे डेविड धवन का एक इंटरव्यू याद है, जिसमें उनकी फिल्मों के बारे में पूछे जाने पर धवन ने कहा था, 'अरे मैं फेलिनी और गोडार्ड देखते हुए बड़ा हुआ हूं। लेकिन वो सब चीज़ें यहाँ नहीं चलेंगी।'
सिंगल-स्क्रीन थिएटर्स मज़ा तो देते थे, लेकिन कई सीमाओं के साथ; और अब मल्टिप्लेक्स के इस दौर में, अनुभव सिन्हा ऐसे कुछ लोगों में से हैं, जो अपनी काबिलियत को साबित करने के लिये दुबारा लौटे हैं; जो अपने बीते हुए कल की असफलता को अब सफलता में बदल रहे हैं।
इसलिये, वो दर्शकों को अपनी सोच से निकाल कर हर छुपी हुई चीज़ परोस रहे हैं -- जिसमें से एक है डायलन की ब्लोइन' इन द विंड की एक झलक, जो अयान रंजन की धूल भरी सड़क पर चलती जीप के साथ दिखाई देती है।
सिन्हा मनोरंजक सामाजिक ड्रामा को बख़ूबी पेश करने में भले ही सफल रहे हों (आर्टिकल 15 मुल्क़ के मुकाबले ज़्यादा सपाट फिल्म है); लेकिन मुझे लगता है कि आज भी वो मुल्क़ से पहले वाले दिनों में उन्हें मिलने वाली तालियों और सीटियों की तलाश में हैं। (तालियाँ पाने के उनके तरीके भले ही बदल गये हों; लेकिन उनकी इच्छा आज भी बनी हुई है)। इसलिये, उनका हुनर तो शानदार है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी वो जोखिम उठाने के लिये तैयार नहीं हैं।
अनुभव सिन्हा की फिल्में हमें भारतीयता के बारे में और भी बहुत कुछ सिखा पातीं -- अगर उन्होंने ख़ुद को सिर्फ शहरी दर्शकों से बांध न लिया होता।
फिलहाल, सिन्हा सिर्फ उन्ही दर्शकों से जुड़ना चाह रहे हैं, जो 'हमारे बीच के अंतर बहुत हुए। आओ समाज में अंतर लायें' जैसी ख़ुशनुमा टैगलाइन्स को दमदार सोच मानते हैं।
उनका हर दृश्य और हर कहानी इन्ही दर्शकों के लिये है।
इन्ही दर्शकों के लिये उन्होंने सामाजिक आँकड़ों से भरे भाषण लिखे हैं।
इन्ही दर्शकों के लिये अंत में उन्होंने आज़ादी का एक तेज़-तर्रार गाना भी डाला है।
अनुभव सिन्हा को स्वीकार करना चाहिये कि उन्हें पता है, जो आसानी से संतुष्ट होने वाले उनके इन दर्शकों को नहीं पता है: आज़ादी विद्रोह का रैप नहीं है। आज़ादी एक दुःखद बैलड है।