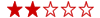'ऐसा लगा जैसे मेरे गले पर कोई फंदा कस रहा हो, और मूवी से मैं कुछ हद तक धोखा खा कर लौटा हूं,' श्रीहरि नायर ने स्वीकार किया।

तुषार हीरानंदानी की सांड की आँख में प्रकाश झा ने एक ऐसा किरदार निभाया है, जिससे सभी दर्शक नफ़रत करेंगे।
महिलाओं पर अत्याचार करने वाला, बच्चों को थप्पड़ मारने वाला और कीमती हुक्के बर्बाद करने वाला आदमी -- ताऊजी की हर बात से नफ़रत की जा सकती है।
ताऊजी के सामने हैं, चंद्रो और प्रकाशी तोमर, जिनकी हर बात अच्छी है।
ये दोनों शार्पशूटर हैं, जिन्हें घर पर प्रताड़ित किया जाता है, जो शूटिंग की प्रतियोगिताओं में छुप कर हिस्सा लेती हैं और पोडियम पर पहला और दूसरा स्थान जीत लेती हैं।
चंद्रो और प्रकाशी का किरदार वास्तविक लोगों पर आधारित है, और एक ईमानदार मूवी यह जानने की कोशिश करती कि क्या इन दोनों महत्वाकांक्षी महिलाओं के बीच कोई तना-तनी थी?
क्योंकि सभी जानते हैं कि जहाँ महत्वाकांक्षा होती है, वहाँ आपसी प्रतिस्पर्धा भी ज़रूर होती है।
लेकिन हमें पर्दे पर फरिश्ते दिखाये गये हैं और उनमें मनुष्यों जैसी कोई भी बात स्कीनराइटिंग को अव्यवहारिक बना सकती थी।
तो इसकी फिक्र ही क्यों करें?
सांड की आँख में हर इंसान या तो नफ़रत से भरे ताऊजी का तरफ़दार है या प्यारी दादियों का समर्थक।
अगर आपको इस तरह के किरदार देखना पसंद है, जिनका अपना कोई व्यक्तित्व न हो, तो आप इस मूवी का आनंद ले सकते हैं।
आप एक उदारपंथी मशीन की तरह पीड़ित बनाम अत्याचारी के इस मुकाबले का मज़ा ले सकते हैं।
मुझसे पूछें, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गले पर कोई फंदा कस रहा हो, और मूवी से मैं कुछ हद तक धोखा खा कर लौटा।
यह उस तरह की मूवी है जिसमें 60 वर्ष की बुढ़िया दिखने के लिये मेकअप से लदी तापसी पन्नू और भूमि पेडणेकर एक शूटिंग प्रतियोगिता में जाती हैं और दर्शक तुरंत उनपर फ़ब्तियाँ कसने लगते हैं -- जैसे उन्होंने दो चुड़ैलों को झाड़ू पर उड़ते देख लिया हो।
दर्शकों का व्यवहार देख कर मैंने ख़ुद से कहा, 'यार, कम से कम मेरी प्रतिष्ठा इन जाहिलों से कहीं ज़्यादा है।'
यही सांड की आँख की 2 घंटे 25 मिनट की कहानी का उद्देश्य है -- यह शहरी, पढ़े-लिखे, सभ्य जैसे लोगों के अहम् को आराम देता है और उन्हें जो भी देखना और सुनना पसंद है, वही दिखाता रहता है।
इसमें कलाकारी और वैसी चीज़ों की कोई जगह नहीं है; जैसे कि यह मूवी डेंटिस्ट्स के लिये बनाई गयी हो।
साथ ही यह उन मूवीज़ में से है, जो आलोचकों को उसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिये ललचा सकती है, जिसका इस्तेमाल फिल्म की प्रचार सामग्री में किया गया है -- अगर हम सावधानी न बरतें, तो यह हम सभी को अपना वफ़ादार पीआर मैनेजर बना सकती है।
'बॉलीवुड हमारे प्रादेशिक सिनेमा को पीछे क्यों धकेल रहा है?' जैसी बातें करने वाले लोग (अगर वे सचमुच इसका जवाब जानना चाहें) साजिद ख़ान की अगली बकवास फिल्म की जगह तुषार हीरानंदानी की फिल्म देखना चाहेंगे।
आज की बेहतरीन भारतीय प्रादेशिक फिल्मों में ज़िंदग़ी की बेकार की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और कहानियों को इन्ही बेकार चीज़ों से उभरने के लिये छोड़ दिया जाता है।
लेकिन सांड की आँख़ में, तोमर देवरानी-भौजाई की जोड़ी के कष्ट को ऐतिहासिक और गंभीर दिखाने के लिये दुनिया अपना रवैया बदलती रहती है।
इस फिल्म में हवा भी बहना बंद कर दे, अगर उसे विनीत कुमार के मसीहा किरदार से यह सुनने को न मिले कि, 'देखो, बदलाव की हवा चल रही है।'
कहानी कुछ ज़्यादा ही सपाट है!
अगर मैं बहुत ज़्यादा ग़ुस्से में लग रहा हूं, तो आपको बता दूं, कि फिल्म की शुरुआत मज़ेदार थी।
पहला अर्धांश काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, इतनी अच्छी तरह कि इसके भीतर छुपा खालीपन हमें दिखाई नहीं देता।
हीरानंदानी की शानदार तकनीक, उनकी आत्मविश्वास से भरी शॉट-टेकिंग और पीड़ित वर्ग की सहनशीलता हमारी दिलचस्पी को बनाये रखती है।
एक ख़ुशनुमा गाने के माध्यम से चंद्रो और प्रकाशी की रोज़ की परेशानियाँ दिखाई गयी हैं, और इसी गाने के माध्यम से उन्हें समझदार औरतों का रूप दिया गया है, जो उनके समाज के मर्दों की उम्मीदों की बेड़ियाँ तोड़ आगे निकल चुकी हैं।
घरेलू दृश्यों में हँसाने वाली मायूसी दिखाई देती है।
तोमर परिवार में तीन जोड़ियाँ एक ही बेडरूम में रहती हैं, जिसके कारण सेक्स समय के अनुसार होता है।
मर्द सिर्फ सेक्स के भूखे निकम्मे हैं, और बच्चों के साथ-साथ खेत को संभालने की ज़िम्मेदारी औरतों की है (एक सीन में तापसी पन्नू बेहद कुशलता से अपने सिर पर ईंटों को ढोती हुई दिखाई देती हैं)।
बाद में जब इमरजंसी लगा दी जाती है और मर्दों की नसबंदी शुरू हो जाती है, तो मर्दों में खलबली मच जाती है, जबकि औरतें मज़ाक उड़ाते हुए सहानुभूति के शब्द कहती दिखाई देती हैं: 'दुःख की बात है कि सरकार मर्दों से वो एक चीज़ भी ले लेना चाहती है, जिसमें वो सचमुच अच्छे हैं।'
हीरानंदानी की सिनेमैटिक पद्धति बेहद बारीक है, और उनकी फ्रेमिंग के साथ-साथ कुछ दृश्यो में भी यह बात साफ़ दिखाई देती है।
मदर इंडिया की एक स्क्रीनिंग में चंद्रो और प्रकाशी अपने घूंघट के भीतर से नरगिस का बंदूकधारी किरदार देखती हैं, और यहीं से उनकी क़िस्मत बदलनी शुरू होती है।
एक सीक्वेंस में जब मैं विनीत कुमार के दिखने की उम्मीद कर रहा था, तभी एक बाइक के आईने में चौंकाने वाले अंदाज़ में उनका चेहरा दिखाई दिया।
जब प्रकाशी और चंद्रो ने घर से दूर रहने के लिये अपने पतियों को झूठी कहानियाँ कहीं, तो उनके डायलॉग्स के बीच का ताल-मेल बिल्कुल सही उभर कर आया।
लेकिन बारीकी और नपे-तुले अंदाज़ के बीच थोड़ा ही अंतर होता है और इसी अंतर के कारण पहले अर्धांश का हल्कापन भारी-भरकम दूसरे अर्धांश के आगे घुटने टेक देता है।
जब दादियाँ जीतने की आदत बना लेती हैं और मूवी को लगता है कि अब समाज में नया दौर लाने का समय आ गया है, तभी से कहानी कमज़ोर, पेशकश टूटी-फूटी और एडिटिंग बेहद तेज़ लगने लगती है।
हीरानंदानी का समाजिक बदलाव एक ऐसे आदमी से आता है, जिसके भीतर आजकल लोकप्रिय हो रहे पुरुष-विरोधी विचारों और ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील लोगों का समर्थन करने वाली हर ख़ूबी है।
लव सोनिया में मनोज बाजपाई का दलाल का किरदार इतना डरावना इसलिये है, क्योंकि मूवी के लेखकों ने उस किरदार को अपनी चालाकी और सूझ-बूझ का इस्तेमाल करने से रोका नहीं था।
आपको उसके इतिहास की झलक दिखाई गयी है और आप जानते हैं कि उसने जो चीज़ें की हैं, उनका कारण क्या है।
प्रकाश झा के साथ खड़े सांड की आँख के सभी पुरुष इतने बेवकूफ़ और मूर्ख लगते हैं कि उनसे ज़रा भी डर नहीं लगता (सच कहूं तो, झा एक मंझे हुए कलाकार हैं, और किरदार की कमज़ोरी का कारण लेखन ही है।)
इन काग़ज़ी शेरों के साथ सही संतुलन बनाने के लिये हीरानंदानी और उनके लेखकों ने हमें कुछ हंस भी दिये हैं, जो बिल्कुल इन्ही के जैसे हैं; पूरी तरह बनावटी।
मैं एक राजसी जोड़ी की बात कर रहा हूं, जो तोमर महिलाओं को एक शूटिंग प्रतियोगिता में मिलती है और फिर उन्हें महल में दावत के लिये बुलाती है।
दावत में जब चंद्रो तोमर अपने हाथ धोने के कटोरे से पानी पी लेती है, तो रानी भी अपने हाथ धोने के कटोरे से पानी पीती है।
यह पूरा दृश्य टेलीविज़न विज्ञापन जैसा लगता है, मानो इसे रीसर्च के आधार पर नहीं, पीयूष पांडे के कहने पर लिखा गया हो।
एक तरह से, सांड की आँख़ जैसी फिल्मों के निर्माता न्यूटन और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों के मुख्य किरदारों की तरह हैं।
यही लोग अपनी उदारता के पर्दे के पीछे से ग्रामीण भारत को देखते हैं और बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं, 'मैं बदलाव लाऊंगा!'
मेरे ख़्याल में न्यूटन और आर्टिकल 15 की सबसे अच्छी बात है इन मुख्य किरदारों की शिक्षा की झलक -- वो पल, जिनमें उन्हें अपने आदर्शवाद का खोखलापन समझ में आता है।
सांड की आँख इन फिल्मों की तरह ख़ुद पर सवाल नहीं उठाती, जिसके कारण इसे उसी घिसी-पिटी तर्ज पर चलना पड़ता है, जिसमें तापसी पन्नू पिछड़े हुए समाज को सही राह दिखाने निकल पड़ती है -- और पॉपकॉर्न प्रेमी ताली बजा कर जिसकी ख़ुशी मना सकते हैं।
इस समय तक फिल्म को देखते रहने का एकमात्र कारण था पन्नू और पेडणेकर द्वारा निभाये गये उनके किरदारों में उनके अभिनय के अंदाज़ को देखना।
और पेडणेकर के परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी तारीफ़ यही होगी कि कुछ समय बाद उस पर ज़रूरत से ज़्यादा पोते गये मेक-अप पर ध्यान नहीं जाता।
उसके भीतर की मंझी हुई अदाकारा ने इस किरदार को स्क्रिप्ट से कहीं बढ़कर अलग रंग दिये हैं।
जब उसने गर्भवती की भूमिका निभाई है, तो उसके चेहरे की थकान उसकी स्थिति को बयाँ करती है।
रोने पर धीरे से ऊपरी होंठ को चबाना।
घबराने पर साँसों का भारीपन महसूस होना।
जब पेडणेकर की चंद्रो तोमर चलती है, तो आपको उसकी चाल में सूजन, हीमोरॉइड्स और बूढ़ी औरत को परेशान कर रहे पाँवों के घठ्ठों का दर्द साफ़ महसूस होता है।
उसने पूरी तरह थियेटर के अंदाज़ में अभिनय परोसा है और इसमें कोई चूक नहीं निकाल सकते।
तापसी पन्नू में मंझी हुई अदाकारा वाले गुर नहीं हैं, लेकिन उसका प्रदर्शन लगातार उभरता आया है।
भूमि के मुकाबले पन्नू का अभिनय थोड़ा कम कुदरती है, और हमेशा की तरह उसने अपने किरदार की उम्मीदों से परे जाने वाली स्थितियों में *संतोषजनक प्रदर्शन* कर दिखाया है।
उसकी ख़ूबसूरत मुस्कुराहट यहाँ काफ़ी काम आयी है -- और फिर भी, मैं सोच रहा था कि रसिका दुगल इस किरदार को कैसे निभाती।
हम बॉलीवुड के उस दौर में जी रहे हैं, जहाँ मसाला इंटरटेनर बनाने के लिये आपको विधवा माँ या बदला लेने वाले बेटे की ज़रूरत नहीं पड़ती।
मौजूदा वातावरण में, भारतीय डायरेक्टर अपनी कहानी में एक सामाजिक मुद्दे को डालकर मूवी में मसाला भरता है और इस सामाजिक मुद्दे के एक ओर बेहद पिछड़े विचारों वाले विलेन और दूसरी ओर बेड़ियाँ तोड़ने के लिये तैयार कुछ पीड़ित लोग ज़रूर होते हैं। (2019 में मसाला सिनेमा ऐसे ही बनता है)।
अगर आप इस तरह की मूवीज़ को झेल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि पहले से ही आपके दिमाग में घर कर चुकी घिसी-पिटी कहानी को देखना मज़ेदार हो सकता है, तो सांड की आँख देखने में आपको तकलीफ़ नहीं होगी।
यह फिल्म मान कर चलती है कि पुरुष-प्रधानता और पुरुषत्व जैसे शब्दों के साथ दर्शकों का ख़राब रिश्ता लेखन की कमियों को दूर कर सकता है और इन कमियों को अनदेखा किया जा सकता है।
इस तरह से देखें, तो सांड की आँख उन ब्लॉकबस्टर्स से अलग नहीं है, जो पिछली दिवालियों में आपका ध्यान खींचने की प्रतिस्पर्धा में लगी थीं।
इस फिल्म में शाहरुख ख़ान, दो हिरोइनें और प्रेम कहानी नहीं है, जो पिछले दशक की दिवाली रिलीज़ेज़ में दिखाई देती थीं। फिर भी यह उतनी ही मीठी, नपी-तुली और आसानी से हज़म होने वाली कहानी है।
बेशक, बदलाव की हवा तो चल पड़ी है।
और हालांकि इनमें मनीष मल्होत्रा के नये कलेक्शन पर लगे पर्फ़्यूम की ख़ुशबू की जगह हमारे गाँवों की महक परोसने की कोशिश की गयी है, लेकिन इसे भी सीधी-सादी सोच वाले दर्शकों को ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।