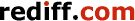 | « Back to article | Print this article |
'ऐल्बर्ट पिन्टो को ग़ुस्सा क्यों आता है न कोई सवाल पूछती है और न ही जवाब देती है,' सुकन्या वर्मा ने गुहार लगाई।

'जितने लोगों ने इस फिल्म को देखा है, उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने इसका नाम सुना है,' नसीरुद्दीन शाह ने अपनी जीवनी ऐंड देन वन डे में लिखा है।
सचमुच, लोग ऐल्बर्ट पिन्टो को ग़ुस्सा क्यूं आता है के नाम और जाने भी दो यारो के समय से पॉप कल्चर में इसकी बढ़ी हुई लोकप्रियता को सईद मिर्ज़ा की आर्ट-हाउस क्लासिक में इसके मुख्य किरदार के ग़ुस्से से कहीं बेहतर जानते हैं।
डायरेक्टर सौमित्रा रानाडे इस श्रेणी में नहीं आते।
मुंबई की टेक्सटाइल मिल्स के माहौल में चल रही मिर्ज़ा की तेज़ कहानी और ईसाई अल्पसंख्यकों के इर्द-गिर्द घूमती चर्चा राजनैतिक जागरुकता और शहरी शोषण की झलक देती है। दुर्भाग्य से, इस मूवी से रानाडे का प्यार एक दमदार रीमेक का रूप नहीं ले पाया है।
ये रीमेक जैसी लगती भी नहीं है, और इसमें असली फिल्म के अंदाज़, लहज़े और सिद्धांतों की बहुत ही कम झलक है।
जहाँ एल्बर्ट पिन्टो को ग़ुस्सा क्यों आता है में विद्रोह की चिंगारी भड़कती दिखाई दी थी, वहीं -- क्यों की जगह क्यूं -- का इस्तेमाल करने वाली ये नयी फिल्म खोखले ग़ुस्से की हिमायत की राह पर भटकती दिखाई देती है।
बिखरे हुए फ़्लैशबैक्स के रूप में रानाडे ने जिस तरह ऐल्बर्ट पिन्टो के ग़ुस्से की झलक दी है उससे पिन्टो के व्यक्तित्व और उसकी सोच की एक टूटी-फूटी, ग़ुस्सा दिलाने वाली तसवीर सामने आती है।
घोटालेबाज़ों की तलाश में सौरभ शुक्ला के साथ सड़क यात्रा पर निकले एल्बर्ट पिन्टो (जिसका किरदार मानव कौल ने निभाया है), एक पुलिस वाले से उसके अचानक ग़ायब होने की बात करते उसके परिवार के लोगों, और बेतरतीब बिखरे फ़्लैशबैक्स के बीच ये स्क्रिप्ट बेढंगी और कमज़ोर लगती है।
नए जमाने के पिंटो के तर्क दुनिया से अलग नहीं हैं।
उसे इस भ्रष्ट, मतलबी दुनिया में बच्चों को जन्म देना सही नहीं लगता।
उसे दुनिया की निष्ठुरता और जगहँसाई का सामना करना पड़ता है। फिल्म में एक पीड़ित आदमी के ग़ुस्से की जगह हमें एक पागल आदमी की उन्मादी बकवास दिखाई देती है।
ऐल्बर्ट पिन्टो ने अपने किरदार को महत्वपूर्ण और वाजिब दिखाने के लिये कड़ी मेहनत की है।
उसकी सड़क यात्रा और उसके सामने आने वाले लोग और उनकी समस्याऍं उसकी उमड़ती सोच के एक सफ़र जैसी लगती हैं। लेकिन कहानी बाल यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर आ जाती है और फिर लापरवाही से उन्हें पीछे छोड़ कर आगे बढ़ जाती है।
गहराई और अपवित्रता के बीच झूलते ऐल्बर्ट पिन्टो का किरदार इतना व्यभिचारी या सनकी नहीं लगता कि हर लड़की में अपनी प्रेमिका को ढूंढने वाली उसकी सोच की उड़ान उसके किरदार से मेल खाये।
साथ ही, मिर्ज़ा की 1980 में बनी फिल्म को देखने वाले लोगों को ज़रूर लगेगा कि रानाडे ने यहाँ बताये गये किरदारों का बख़ूबी वर्णन नहीं किया है।
ऐल्बर्ट पिन्टो को ग़ुस्सा क्यों आता है में गंभीर कमियाँ होने के बावजूद, इसके अभिनेताओं ने काफ़ी हद तक इसे पूरी तरह बनावटी बनने से बचा लिया है।
मानव कौल के ग़ुस्से का आधार न होने के बावजूद उसका संजीदा अभिनय अपनी छाप छोड़ने में सफल रहा है।
वो ऐल्बर्ट, अक़बर या अमर कोई भी हो सकता था, उसका धर्म कतई मायने नहीं रखता।
नंदिता दास अपने किरदार से कहीं ज़्यादा समझदार लगती हैं, लेकिन उनकी सादग़ी भरी अदा कमियों को काफ़ी हद तक छुपा देती है।
लेकिन फिल्म की इस भटकी हुई कहानी में जिस तरह से सौरभ शुक्ला ने घिनौनी चरित्रहीनता को अपने किरदार में बख़ूबी पिरोया है, वह सचमुच काबिले तारीफ़ है।
माहौल बदलता है, समस्याऍं बदलती हैं, लेकिन ऐल्बर्ट पिन्टो हार और निराशा के कभी न ख़त्म होने वाले चक्र में फँसा ही रहता है।
रानाडे इस किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाये हैं।
प्रासंगिकता पर्याप्त नहीं है।
प्रतिक्रिया भी तो ज़रूरी है।
ऐल्बर्ट पिन्टो को ग़ुस्सा क्यों आता है न कोई सवाल पूछती है और न ही जवाब देती है।